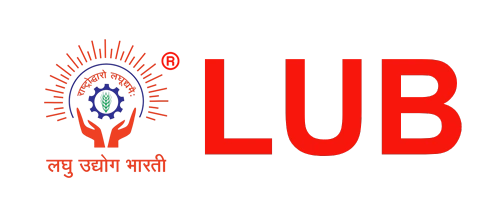आज भारत अपनी सबसे युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाने के लिए प्रयासरत है। विकासशील देश के टैग को हटाने और विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षा को खुले तौर पर प्रकट करने के बाद उन कमियों को दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच बड़ा अंतर करती हैं। इस बदलाव के लिए भारत के विकास की नई सोच और दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे युवाओं की है।
भारत में युवाओं की संख्या दुनिया के अधिकांश देशों से कहीं अधिक है, और यह युवा शक्ति देश के समग्र विकास का आधार बन सकती है। कौशल की कमी के कारण हमारे पास अपार युवा संसाधन होते हुए भी न तो उन्हें उचित रोजगार के अवसर मिल पाते हैं, और न ही उद्योगों को योग्य और कुशल कार्यबल। यह स्थिति न केवल युवाओं के लिए, बल्कि देश की समग्र विकास प्रक्रिया के लिए भी एक चुनौती बन जाती है। यही कारण है कि भारत के लिए कौशल विकास अब न केवल अवसर है, बल्कि आवश्यकता बन चुका है।
कौशल विकास के वैश्विक रुझान और उनका प्रभाव-वर्तमान समय में, कौशल विकास वैश्विक मेगा रुझानों के केंद्र में है, जैसे स्वचालन, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई, उत्पादों और सेवाओं का डिजिटलीकरण, और सिकुड़ती श्रम शक्ति। इन सभी परिवर्तनों का सीधे तौर पर प्रभाव शिक्षा और श्रम बाजारों पर पड़ रहा है, जो काम और कौशल की मांग की प्रक्ति को बदल रहे हैं। इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखना और अपने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।
कौशल और कार्यबल विकास प्रणालियों को अब इन बदलावों के लिए सक्रिय रूप से अनुकूल होना चाहिए। स्वचालन और डिजिटलीकरण के कारण श्रमिकों की आवश्यकताएँ लगातार बदल रही हैं, और ऐसी स्थिति में, वैश्विक स्तर पर शिक्षा और कार्यबल विकास प्रणालियों के प्रतिमान को फिर से परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। भविष्य के श्रम बाजार में, शिक्षा और कौशल प्रणालियों को अधिक व्यक्तिगत, सुलभ (दूरस्थ और संकर शिक्षा की अनुमति देते हुए) और निरंतर रूप से कार्यकर्ता के करियर के दौरान विकसित होने वाला होना चाहिए।
दुनियाभर की सरकारों के एजेंडे में कौशल विकास-
कौशल विकास का एजेंडा आज दुनियाभर की सरकारों की पहली प्राथमिकता में हैं। हम पश्चिम और विकसित राष्ट्रों को कितना भी कोर्से, लेकिन स्किल्स के मामले में वे हमसे बहुत आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व बैंक (World Bank) जैसे संगठनों ने कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किए हैं। विश्व बैंक को 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, “Skills for a Changing World” पहल के तहत विकासशील देशों में कौशल विकास परियोजनाओं के लिए 6 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया। इसी तरह, यूरोपीय संघ ने 2023 में “Digital Europe Program” के तहत डिजिटल कौशल को सशक्त बनाने के लिए 580 मिलियन का बजट निर्धारित किया।
टेक्नोलॉजी हब्स और डिजिटल लैब्स यूरोप, अमेरिका और एशिया में डिजिटल स्किल हब्स स्थापित किए गए हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Coursera, edX और Skillshare जैसे प्लेटफॉर्म ने कौशल विकास को दूरस्थ और सुलभ बनाया है। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम वैश्विक कंपनियों ने विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के AI, मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस में ट्रेनिंग कार्यक्रम।
पौराणिक काल से भारत में कौशल का महत्व
भारतीय संस्कृति और दर्शन में कौशल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे प्राचीन काल से ही जीवन के एक अनिवार्य तत्व के रूप में माना गया है। हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण को 14 विद्याओं और 64 कलाओं में पारंगत माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपनी सम्पूर्ण शिक्षा और ज्ञान उज्जैन में गुरु संदीपनि के आश्रम में प्राप्त की। श्री कृष्ण के साथ यहाँ उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम भी थे। माना जाता है कि यही स्थान विश्व का पहला गुरुकुल था। श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिनों में ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और इन कलाओं में से अधिकांश कलाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आज के समय में कौशल के रूप में मानते हैं।
इन कलाओं में न केवल बेताल को वश में करना, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, मंत्र विद्या, जल को बांधना, इंद्रजाल-जादूगरी और इच्छाधारी वेष धारण करने जैसी विलक्षण विद्या शामिल थीं, बल्कि अन्य सामान्य कौशल भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, नृत्य, वाद्य बजाना, गायन, नाट्य-अभिनय, पकवान कला, कपड़े और गहने बनाना, चित्रकारी, कूटनीति, और शंख व हाथी दांत से गहने तैयार करना। इन कलाओं के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौशल या स्किल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह केवल जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान करता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित यह 64 कलाएं न केवल शारीरिक या मानसिक कौशल से संबंधित थीं, बल्कि वे एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास का प्रतीक थीं।
कौशल विकास के नए आयाम-
कई देशों में, विशेष रूप से LMIC (लो और मिडल इनकम कंट्रीज) में, कौशल प्रणालियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कई श्रमिक फीलांसिंग, अनौपचारिक नौकरियों या स्वरोजगार में संलग्न होंगे। ऐसे श्रमिकों को भी अधिक लाभदायक, उत्पादक और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
सफलता के लिए ये कौशल हैं जरूरी-
21वीं सदी के श्रम बाजार में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को व्यापक कौशल सेट की आवश्यकता होती है। इनमें बुनियादी और उच्च क्रम कौशल शामिल हैं, जो संज्ञानात्मक कौशल हैं। ये कौशल जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के लिए प्रभावी ढंग से अनुकूल होने, अनुभव से सीखने और तर्क करने की क्षमता को परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-भावनात्मक कौशल, विशेष कौशल और डिजिटल कौशल भी आवश्यक हैं।
बुनियादी और उच्च क्रम कौशल ये संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, जो व्यक्ति को जटिल समस्याओं को हल करने और नए विचारों को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं।
सामाजिक भावनात्मक कौशल यह कौशल किसी व्यक्ति को रिश्तों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इनमें नेतृत्व, टीमवर्क, आत्म-नियंत्रण और धैर्य जैसे गुण शामिल हैं।
विशेष कौशल में किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यक होते हैं और इनमें तकनीकी और संज्ञानात्मक कौशल के साथ-साथ उद्यमिता कौशल भी शामिल हैं।
डिजिटल कौशल ये सभी प्रकार के कौशलों के ऊपर आधारित होते हैं और जानकारी तक सुरक्षित पहुँच, उसका प्रबंधन, समझ, और निर्माण की क्षमता को परिभाषित करते हैं।
कौशल विकास की दिशा में दो कदम-
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, इस दिशा में गंभीर प्रयास किए गए हैं। भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, ताकि हमारी युवा शक्ति को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जा सके।
वर्ष 2047 तक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत को स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल बेरोजगारी से निपटने के लिए नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। अगर हम अपने युवाओं को कौशल से लैस करने में सफल होते हैं, तो यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ (PMKVY) जैसे कार्यक्रम इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को विभित्र क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे कामकाजी दुनिया में सफल हो सकें। इसी तरह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इससे न केवल बेरोजगारी की रफ्तार में कमी आएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत युवाओं को डिजिटल तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के जरिये युवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
भारत में कौशल विकास चुनौतियां और समाधान
भारत की युवा जनसंख्या के लगातार बढ़ते आकार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रमुख भूमिका को देखते हुए, कौशल विकास को लेकर देश में कई रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य भारत को एक प्रमुख कौशल हब के रूप में स्थापित करना है, जहाँ प्रशिक्षित युवाओं का योगदान वैश्विक कार्यवल में महत्वपूर्ण हो।
कौशल विकास में प्रमुख चुनौतियां-
असमान शिक्षा और कौशल स्तर भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा और कौशल विकास सुविधाओं में बड़ा अंतर है। यह असमानता ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने में बाधक बनती है, जो उनके रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है।
अप्रचलित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रणाली- वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम उद्योग की बदलती आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। इस कारण से कई युवा प्रशिक्षित होने के बावजूद रोजगार के लिए तैयार नहीं होते हैं।
वित्तीय बाधाएं-
कई युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की लागत वहन करना कठिन होता है, जिससे वित्तीय सहायता और सब्सिडी की आवश्यकता बढ़ जाती है।
अधूरी उद्योग-शिक्षा भागीदारी-
उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग की कमी के कारण छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त नहीं होता, जो उन्हें वास्तविक कार्य परिस्थितियों में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
कम जागरूकता-
विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग में कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता की कमी है, जिससे ये वर्ग इन अवसरों से वंचित रह जाता है।
महिला भागीदारी में कमी-
सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं की कौशल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी सीमित होती है, जिससे उनके रोजगार के अवसरों में कमी आती है।
समाधान
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कौशल विकास केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके दूरदराज क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।
पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण कौशल विकास पाठ्यक्रमों को उद्योग की वर्तमान और भविष्य की मांग के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
वित्तीय सहायता और सब्सिडी सरकारी और निजी क्षेत्र को छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में छात्रवृत्तियाँ और त्रऋण योजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग से छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का अनुभव मिल सकता है, जो उनकी व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाएगा।
जागरूकता अभियान कौशल विकास के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।